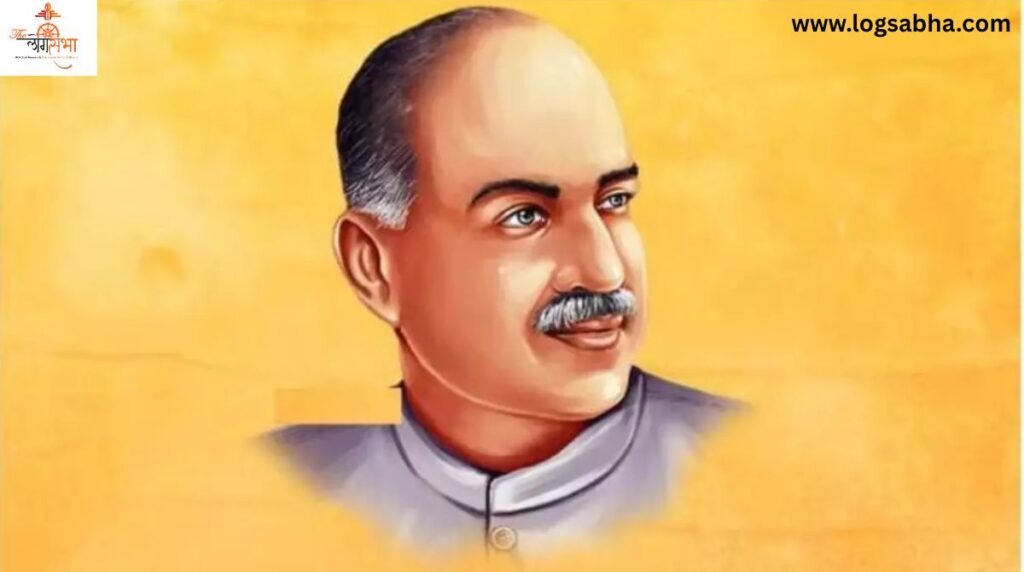कुछ मौतें इतिहास के शांत गलियारों में खो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता।
23 जून 1953 की सुबह, 51 वर्षीय एक राष्ट्रवादी नेता श्रीनगर में नजरबंदी के दौरान मृत पाए गए—घर से दूर, संसद से दूर और उन लोगों से दूर, जिनका प्रतिनिधित्व करने की उन्होंने शपथ ली थी। आधिकारिक बयान संक्षिप्त था: हृदयाघात। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, वह और भी भारी था। न कोई पोस्टमार्टम। न पारदर्शी जांच। न स्पष्ट निष्कर्ष। स्वतंत्रता के केवल छह वर्ष बाद, देश के एक प्रमुख विपक्षी नेता की हिरासत में मृत्यु हो गई और गणराज्य ठोस उत्तर देने में असमर्थ रहा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने समय की सबसे शक्तिशाली सरकार को खुली चुनौती दी थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे पर सवाल उठाए, परमिट व्यवस्था का विरोध किया और अनुच्छेद 370 की राजनीतिक संरचना का खुलकर प्रतिरोध किया। उनका नारा—“एक निशान, एक विधान, एक प्रधान”—सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं था; वह सत्तारूढ़ व्यवस्था के लिए एक सीधी वैचारिक चुनौती था। कुछ ही सप्ताह बाद, वे नहीं रहे।
क्या यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चिकित्सकीय विफलता थी? क्या यह लापरवाही थी, जो प्रशासनिक उदासीनता के पीछे छिप गई? या फिर एक नवजात लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को दबा दिया गया?
ये प्रश्न सात दशकों से अधिक समय से अनुत्तरित हैं—मानो राष्ट्र की राजनीतिक स्मृति में एक अधूरा घाव बनकर रह गए हों। यह केवल एक मृत्यु की कहानी नहीं है। यह संदेह, सत्ता, जवाबदेही और एक युवा लोकतंत्र की कठिन परीक्षा की कहानी है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी: जीवन और व्यक्तित्व
श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक भारत के सबसे प्रभावशाली और बौद्धिक रूप से प्रखर नेताओं में से एक थे। वे एक विद्वान, बैरिस्टर, सांसद और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश में संगठित राजनीतिक विपक्ष की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) में हुआ। 23 जून 1953 को श्रीनगर में विवादास्पद परिस्थितियों में उनका निधन हुआ। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की — वही संगठन, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रूप में विकसित हुआ।
उनका जीवन शिक्षा और राजनीति — दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक एकता के प्रबल समर्थक थे। बंगाल के विभाजन का विरोध और अनुच्छेद 370 के खिलाफ उनका अभियान उनकी विरासत के प्रमुख आयाम हैं।
प्रारंभिक जीवन और शैक्षणिक उपलब्धियाँ
श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रतिष्ठित बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता, सर आशुतोष मुखर्जी, प्रसिद्ध विधिवेत्ता और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वे भारत में उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए जाने जाते थे। ऐसे बौद्धिक वातावरण में पले-बढ़े मुखर्जी ने विद्वता, अनुशासन और राष्ट्रीय गर्व के मूल्य आत्मसात किए।
उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं—
-
प्रेसीडेंसी कॉलेज से अंग्रेज़ी में बी.ए. (ऑनर्स)
-
बंगला में एम.ए.
-
विधि स्नातक (एल.एल.बी.)
-
1927 में लंदन के लिंकन इन से बैरिस्टर
केवल 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने (1934–1938)। अपने कार्यकाल में उन्होंने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया, शोध संस्थानों को सुदृढ़ किया और भारतीय इतिहास व संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित किया।
राजनीतिक यात्रा और राष्ट्रवादी भूमिका
मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा बंगाल की विधान परिषद से शुरू हुई। 1930 के दशक के अंत तक वे हिंदू महासभा से जुड़ गए और बाद में उसके अध्यक्ष बने। उस समय देश साम्प्रदायिक तनाव और औपनिवेशिक अस्थिरता से गुजर रहा था। उन्होंने हिंदू राजनीतिक एकजुटता और राष्ट्रीय एकता की वकालत की।
स्वतंत्रता से पहले के वर्षों में—
-
उन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया और इसे क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक बताया।
-
1941–1942 के दौरान वे बंगाल सरकार में वित्त मंत्री रहे।
-
1947 में उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत में बनाए रखने के लिए सक्रिय अभियान चलाया।
स्वतंत्र भारत में भूमिका और कांग्रेस से मतभेद
स्वतंत्रता के बाद वे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। इस पद पर उन्होंने नवस्वतंत्र भारत की प्रारंभिक औद्योगिक नीति के निर्माण में योगदान दिया।
हालाँकि, वैचारिक मतभेद उभरने लगे। 1950 में उन्होंने नेहरू-लियाकत समझौते का विरोध करते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया। उनका तर्क था कि यह समझौता पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता। यह इस्तीफ़ा उन्हें मंत्री से प्रमुख विपक्षी नेता की भूमिका में ले आया।
भारतीय जनसंघ की स्थापना (1951)
अक्टूबर 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थन से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रभुत्व के समक्ष एक संगठित राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना था।
पार्टी के प्रमुख सिद्धांत थे—
-
राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक समरसता
-
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
-
आर्थिक आत्मनिर्भरता
-
समान नागरिक संहिता की वकालत
-
अनुच्छेद 370 का विरोध
उनके नेतृत्व में जनसंघ ने वैचारिक और संगठनात्मक आधार तैयार किया, जो आगे चलकर भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक धाराओं में से एक बना।
कश्मीर आंदोलन और असमय निधन (1953)
मुखर्जी का सबसे विवादास्पद और निर्णायक अभियान जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे के विरोध में था। उन्होंने नारा दिया—
“एक निशान, एक विधान, एक प्रधान”
मई 1953 में उन्होंने अलग परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए बिना अनुमति जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को हिरासत में उनका निधन हो गया। आधिकारिक कारण हृदयाघात बताया गया, किंतु चिकित्सकीय लापरवाही और अन्य प्रश्नों को लेकर दशकों तक संदेह बना रहा।
विरासत और ऐतिहासिक मूल्यांकन
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत बहुआयामी और प्रभावशाली है।
स्थायी योगदान
-
कांग्रेस के प्रभुत्व के विरुद्ध संगठित वैचारिक विपक्ष की स्थापना
-
भारतीय जनसंघ की नींव रखी, जो आगे चलकर भाजपा बनी
-
राष्ट्रीय एकीकरण और संवैधानिक एकता के पक्षधर
-
शिक्षा सुधार और बौद्धिक आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया
बहस और आलोचनाएँ
-
हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति से जुड़ाव को लेकर आलोचना
-
स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ चरणों में उनकी भूमिका पर इतिहासकारों के बीच मतभेद
फिर भी, राजनीतिक दृष्टिकोण चाहे जो हो, भारत की राजनीतिक यात्रा पर उनका प्रभाव निर्विवाद है।
विचारों के निर्माता, लोकतंत्र के शिल्पी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं थे; वे संस्थाओं और विचारों के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय पहचान को नई दिशा देने का प्रयास किया और सांस्कृतिक आस्था तथा संवैधानिक एकता पर आधारित एक संगठित राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की कोशिश की।
उनका जीवन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने विपक्ष की राजनीति को आकार दिया, राष्ट्रीय एकीकरण पर होने वाली बहसों को प्रभावित किया और समकालीन भारतीय राजनीति की वैचारिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया।
1934: श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति
1934 में, मात्र 33 वर्ष की असाधारण आयु में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। वे इस पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। यह नियुक्ति उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने उन्हें एक प्रतिभाशाली विद्वान और बैरिस्टर से राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले शैक्षणिक नेता में बदल दिया।
वे अपने पिता, सर आशुतोष मुखर्जी, की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, जिनका कार्यकाल भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। किंतु श्यामा प्रसाद की नियुक्ति केवल पारिवारिक विरासत के कारण नहीं थी। उस समय तक वे अंग्रेज़ी और बंगला में उच्च डिग्रियाँ प्राप्त कर चुके थे, भारत और लंदन के लिंकन इन में विधि का प्रशिक्षण ले चुके थे और बंगाल विधान परिषद के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे।
यद्यपि कुछ वर्गों में उनकी कम आयु को लेकर संदेह था, परंतु समय ने इस नियुक्ति को दूरदर्शी सिद्ध किया।
सुधारवादी नेतृत्व (1934–1938)
चार वर्षों के अपने कार्यकाल में मुखर्जी ने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक उत्कृष्टता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास — दोनों को मजबूत करने पर ध्यान दिया।
उन्होंने उच्च शिक्षा में बंगला भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया, ताकि शिक्षा भारतीय भाषाई पहचान से जुड़ सके और अधिक सुलभ बने। उस समय जब औपनिवेशिक प्रभाव बौद्धिक संस्थानों पर गहरा था, यह कदम शैक्षणिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण था।
उन्होंने भारतीय इतिहास, दर्शन और पारंपरिक ज्ञान पर अनुसंधान को प्रोत्साहित किया, साथ ही पाठ्यक्रमों को आधुनिक वैश्विक विकास के अनुरूप अद्यतन किया। उनके नेतृत्व में शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ किया गया, वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित किया गया और छात्र कल्याण योजनाओं का विस्तार किया गया।
मुखर्जी का मानना था कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्रीधारक तैयार करना नहीं, बल्कि चरित्र, बौद्धिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना होना चाहिए।
शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के बीच सेतु
यद्यपि उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका बाद में स्पष्ट रूप से सामने आई, पर कुलपति के रूप में उनका कार्यकाल उन्हें विद्वत्ता और सार्वजनिक नेतृत्व के संगम पर ले आया। देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का संचालन करते हुए उन्होंने प्रशासनिक अनुभव, रणनीतिक दृष्टि और सार्वजनिक विश्वसनीयता अर्जित की—ये गुण आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की आधारशिला बने।
उनका कार्यकाल इस बात का उदाहरण था कि अनुशासन और बौद्धिक स्पष्टता से युक्त युवा नेतृत्व भी स्थापित संस्थानों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर सकता है।
संस्था से राष्ट्र तक की यात्रा
कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी; यह उस नई भारतीय नेतृत्व पीढ़ी के उभार का प्रतीक थी, जो आत्मविश्वासी, सुधारवादी और सांस्कृतिक रूप से सजग थी।
1938 में जब उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पद छोड़ा, तब तक वे विद्वता और प्रशासन को सफलतापूर्वक जोड़ने की अपनी क्षमता सिद्ध कर चुके थे। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें मंत्री, राष्ट्रवादी नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक के रूप में स्थापित करने में सहायक बना।
सारतः, 1934 वह वर्ष था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मंच पर उभरे—आंदोलन के माध्यम से नहीं, बल्कि संस्था-निर्माण, सुधार और वैचारिक प्रतिबद्धता के माध्यम से।
1939: हिंदू महासभा में प्रवेश
1939 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औपचारिक रूप से अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़ने का निर्णय लिया। यह उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ था। इससे पहले वे एक विद्वान, विधिवेत्ता और स्वतंत्र विधायक के रूप में सम्मानित थे। इस कदम के साथ उन्होंने स्वयं को संगठित हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति से स्पष्ट रूप से जोड़ लिया, जिसने आगे चलकर उनके सार्वजनिक जीवन की वैचारिक दिशा तय की।
राजनीति का उथल-पुथल भरा दौर
1930 के दशक के अंत तक ब्रिटिश भारत में साम्प्रदायिक तनाव और संवैधानिक अनिश्चितता बढ़ रही थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों ने विशेषकर बंगाल में प्रतिस्पर्धी राजनीति को तीव्र कर दिया था। मुस्लिम लीग अलग राजनीतिक संरक्षण की मांग को मजबूत कर रही थी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व व्यापक राष्ट्रीय गठबंधन बनाए रखने का प्रयास कर रहा था।
बंगाल विधान परिषद में दो बार स्वतंत्र सदस्य के रूप में चुने गए मुखर्जी को यह महसूस होने लगा कि बंगाल की बदलती राजनीतिक संरचना में हिंदू समुदाय की राजनीतिक चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति, विशेषकर मुस्लिम लीग के साथ उसकी बातचीत की दिशा, उन्हें संतोषजनक नहीं लगी। यही असंतोष उन्हें अधिक स्पष्ट वैचारिक मंच की ओर ले गया।
हिंदुत्व विचारधारा का प्रभाव
उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष विनायक दामोदर सावरकर ने “हिंदुत्व” को भारतीय राष्ट्रत्व की एक सभ्यतागत रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया था। मुखर्जी को इस विचार में गहरी समानता महसूस हुई कि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक निरंतरता में निहित है।
1939 में उन्होंने औपचारिक रूप से हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की और शीघ्र ही संगठन में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। उनकी बौद्धिक प्रतिष्ठा, प्रशासनिक अनुभव और प्रभावशाली वक्तृत्व शैली ने विशेष रूप से बंगाल में महासभा की विश्वसनीयता को मजबूत किया। वे शीघ्र ही कार्यकारी अध्यक्ष बने और संगठन की राजनीतिक व रणनीतिक दिशा का नेतृत्व करने लगे।
नीति, मतभेद और निर्णय
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुखर्जी ने 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का समर्थन नहीं किया। उनका तर्क था कि युद्धकाल में अचानक प्रशासनिक शून्य उत्पन्न होने से अस्थिरता और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इसके स्थान पर उन्होंने राजनीतिक संगठन को मजबूत करने और समुदाय के हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।
1941 से 1943 के बीच वे बंगाल की गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री रहे। उनका कार्यकाल आर्थिक अस्थिरता और बंगाल के अकाल के समय से जुड़ा था। नीतिगत मतभेदों के कारण उन्होंने अंततः पद से इस्तीफ़ा दे दिया।
जब विभाजन की चर्चा तेज़ हुई, तब मुखर्जी बंगाल के विभाजन के प्रश्न पर मुखर हो गए। प्रारंभ में उन्होंने पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल किए जाने का विरोध किया। जब विभाजन लगभग निश्चित हो गया, तब उन्होंने भारत के भीतर एक हिंदू-बहुल पश्चिम बंगाल के निर्माण की वकालत की। इस रुख ने 1947 में अंतिम भू-सीमा निर्धारण को प्रभावित किया।
ऐतिहासिक महत्व
1939 का निर्णय कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था—
-
संवैधानिक उदार रुख से वैचारिक राजनीति की ओर उनका स्पष्ट झुकाव
-
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सुदृढ़ होना
-
1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की वैचारिक नींव
हिंदू महासभा ने उन्हें राजनीतिक अनुभव और वैचारिक स्पष्टता प्रदान की, यद्यपि बाद में संगठनात्मक सीमाओं के कारण उन्होंने एक व्यापक राजनीतिक मंच स्थापित करने का निर्णय लिया।
संक्षेप में, 1939 वह वर्ष था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बौद्धिक भागीदारी से आगे बढ़कर वैचारिक नेतृत्व की भूमिका में आए—एक ऐसा परिवर्तन जिसने आने वाले दशकों तक उनकी राजनीतिक विरासत को आकार दिया।
1946–1947: बंगाल के विभाजन पर मुखर्जी की भूमिका
स्वतंत्रता से पहले के वर्ष अनिश्चितता, साम्प्रदायिक अशांति और तीव्र राजनीतिक वार्ताओं से भरे हुए थे। इसी उथल-पुथल के बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के भविष्य पर होने वाली बहस के केंद्रीय व्यक्तित्व बनकर उभरे। पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल किए जाने का उनका विरोध और बाद में विभाजित बंगाल की वकालत उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक अध्याय बना।
राजनीतिक और साम्प्रदायिक परिप्रेक्ष्य
1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक संवैधानिक योजना प्रस्तावित की, जिसमें प्रांतों को जनसंख्या संरचना के आधार पर समूहों में बांटा गया। बंगाल, जहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी थी, उस समूह में रखा गया जिसे मुस्लिम लीग के प्रभाव की ओर झुकता हुआ माना जा रहा था।
16 अगस्त 1946 के ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ के बाद कलकत्ता और नोआखाली में भड़की हिंसा ने समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। पाकिस्तान की मांग तेज़ हो रही थी और मुस्लिम लीग पूरे बंगाल को नए राष्ट्र में शामिल करना चाहती थी।
कुछ नेताओं ने एक स्वतंत्र और संयुक्त बंगाल का प्रस्ताव भी रखा, जो न भारत का हिस्सा हो और न पाकिस्तान का। मुखर्जी ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में हिंदू समुदाय राजनीतिक रूप से असुरक्षित हो जाएगा।
विभाजन की ओर झुकाव
प्रारंभ में वे संयुक्त संरचना के भीतर हिंदू हितों की सुरक्षा चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक हाशिए पर जाने से बचने के लिए विभाजन ही व्यावहारिक समाधान है।
उन्होंने जनसंख्या के आधार पर बंगाल के विभाजन की मांग की, ताकि हिंदू-बहुल क्षेत्र भारत में बने रहें। उनके तर्क तीन मुख्य चिंताओं पर आधारित थे—
-
राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक नियंत्रण
-
सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं की सुरक्षा
-
अल्पसंख्यक समुदायों की दीर्घकालिक सुरक्षा
जनमत और वार्ताएँ
मुखर्जी ने भाषणों, बैठकों और प्रेस के माध्यम से जनमत को संगठित किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और ब्रिटिश अधिकारियों के सामने जनसंख्या आँकड़ों और संवैधानिक तर्कों को रखा। जैसे-जैसे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा, उनके विचारों को व्यापक समर्थन मिलने लगा।
1947 के मध्य तक कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन को स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत—
-
पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना
-
पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हुआ (जो बाद में बांग्लादेश बना)
विभाजन की विरासत
बंगाल विभाजन के प्रश्न पर मुखर्जी की भूमिका ने अंतिम सीमाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समर्थकों के अनुसार, उनके प्रयासों ने हिंदू-बहुल क्षेत्रों को भारत में बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। आलोचकों का मत है कि विभाजन की राजनीति, चाहे उसे किसी ने भी समर्थन दिया हो, उपमहाद्वीप में व्यापक विस्थापन और हिंसा का कारण बनी।
दीर्घकालिक प्रभाव
बंगाल प्रकरण ने मुखर्जी के इस विश्वास को और मजबूत किया कि सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक संगठन आपस में गहराई से जुड़े हैं। यही सोच आगे चलकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना में दिखाई दी और स्वतंत्र भारत की राष्ट्रवादी राजनीति की वैचारिक दिशा को प्रभावित किया।
संक्षेप में, 1946–1947 का कालखंड उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ था। बंगाल विभाजन पर उनकी भूमिका ने न केवल प्रांत की नियति को बदला, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख चेहरों में स्थापित किया।
1947–1950: स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में भूमिका
15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा निर्णय लिया जिसने समर्थकों और आलोचकों दोनों को चौंका दिया। हिंदू महासभा के प्रमुख नेता और कांग्रेस की नीतियों के मुखर आलोचक होने के बावजूद, उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निमंत्रण स्वीकार कर स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया।
कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार में उनका प्रवेश विभाजन के बाद गहरे आघात से जूझ रहे राष्ट्र में एकता का संकेत था।
नेहरू ने उन्हें क्यों आमंत्रित किया
स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा था—विस्थापन, साम्प्रदायिक हिंसा, खाद्य संकट, प्रशासनिक अव्यवस्था और आर्थिक अस्थिरता। नेहरू एक ऐसी मंत्रिपरिषद बनाना चाहते थे जो समावेशी और स्थिर दिखाई दे।
मुखर्जी को शामिल करने के पीछे कई कारण थे—
-
वे एक सम्मानित विद्वान और प्रशासक थे।
-
वे कांग्रेस से बाहर की राष्ट्रवादी धारा का प्रतिनिधित्व करते थे।
-
वे एक प्रमुख बंगाली नेता थे, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बना।
-
उनकी उपस्थिति तत्काल वैचारिक ध्रुवीकरण को कम करने में सहायक हो सकती थी।
माना जाता है कि महात्मा गांधी ने भी मंत्रिमंडल में व्यापक प्रतिनिधित्व के पक्ष में सुझाव दिया था।
मंत्री के रूप में कार्य
उद्योग और आपूर्ति (बाद में वाणिज्य सहित) मंत्री के रूप में मुखर्जी ने विभाजन के बाद की कठिन आर्थिक परिस्थितियों में भूमिका निभाई। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल था—
-
औद्योगिक उत्पादन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन
-
काला बाज़ारी और अभाव की स्थिति से निपटना
-
शरणार्थियों के पुनर्वास में सहयोग
-
प्रारंभिक औद्योगिक नीति पर विमर्श में भागीदारी
यद्यपि वे नेहरू की समाजवादी दृष्टि से पूर्णतः सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक अनुशासित मंत्री के रूप में प्रशासनिक दक्षता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।
वैचारिक मतभेद गहराते हैं
1949–1950 तक गंभीर मतभेद उभर आए।
मुख्य विवाद के क्षेत्र थे—
-
नेहरू–लियाकत समझौता (1950): उनका मानना था कि यह समझौता पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता।
-
कश्मीर नीति: उन्होंने अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों का विरोध किया और इसे अत्यधिक रियायत माना।
-
अल्पसंख्यक और शरणार्थी नीति: उनका मत था कि विस्थापित समुदायों की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक दृढ़ रुख अपनाना चाहिए।
ये केवल नीतिगत मतभेद नहीं थे; ये राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्षता और राज्य की भूमिका को लेकर मूलभूत दृष्टिकोणों का अंतर थे।
इस्तीफ़ा: एक निर्णायक मोड़
6 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे पूर्वी बंगाल और कश्मीर से जुड़ी सरकार की नीतियों का समर्थन नहीं कर सकते।
उनका इस्तीफ़ा कांग्रेस से वैचारिक दूरी का स्पष्ट संकेत था और राष्ट्रवादी दक्षिणपंथ से संगठित विपक्ष की राजनीति की शुरुआत भी।
एक वर्ष के भीतर, अक्टूबर 1951 में, उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की—एक संगठित राजनीतिक विकल्प, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुआ।
सहयोग से टकराव तक
मंत्रिमंडल में मुखर्जी का कार्यकाल स्वतंत्र भारत में वैचारिक सह-अस्तित्व के शुरुआती प्रयासों में से एक था। उनका इस्तीफ़ा उस प्रयोग की सीमाओं को दर्शाता है और आने वाले दशकों के राजनीतिक पुनर्संरचना का आधार बनता है।
1947–1950 का कालखंड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है—जहाँ सहयोग और विरोध के बीच की रेखा स्पष्ट हुई और जिसने भारत में केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीति की दिशा तय की।
1951: भारतीय जनसंघ की स्थापना
21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ (BJS) की स्थापना की। यह केवल एक नई पार्टी का गठन नहीं था; यह स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के सामने एक संगठित राष्ट्रवादी विकल्प का औपचारिक उदय था।
पृष्ठभूमि और उद्देश्य
अप्रैल 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफ़े के बाद मुखर्जी सरकार की नीतियों से निराश थे, विशेषकर—
-
नेहरू–लियाकत समझौता, जिसे वे पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा के लिए अपर्याप्त मानते थे।
-
अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष संवैधानिक दर्जा।
-
राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्न पर कांग्रेस का अपेक्षाकृत नरम रुख।
साथ ही, हिंदू महासभा के पास लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संगठनात्मक विस्तार नहीं था। मुखर्जी ने महसूस किया कि एक व्यापक, अनुशासित और जनाधार वाली राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता है, जो भारतीय सांस्कृतिक पहचान पर आधारित हो और संवैधानिक लोकतंत्र के भीतर काम कर सके।
गठन और वैचारिक दिशा
भारतीय जनसंघ को निम्न सिद्धांतों के साथ स्थापित किया गया—
-
राष्ट्रीय एकता और पूर्ण क्षेत्रीय एकीकरण
-
आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सिद्धांत
-
समान नागरिक संहिता
-
भारतीय सभ्यता पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
-
मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्रीकृत संप्रभुता
मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। दीनदयाल उपाध्याय को संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीनी स्तर पर कैडर समर्थन प्रदान किया।
प्रारंभिक चुनावी उपस्थिति
1951–52 के आम चुनावों में जनसंघ ने लोकसभा की तीन सीटें जीतीं और कुछ राज्यों की विधानसभाओं में सीमित सफलता प्राप्त की। यद्यपि उसकी संसदीय ताकत सीमित थी, पर वह कांग्रेस के सामने एक संगठित वैचारिक विपक्ष के रूप में स्थापित हो गया।
दक्षिणपंथी राजनीति की शुरुआत
जनसंघ की स्थापना ने स्वतंत्र भारत में संगठित दक्षिणपंथी राजनीति की शुरुआत की। इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में संस्थागत रूप दिया और आने वाले दशकों में प्रभाव बढ़ाने वाली राजनीतिक धारा को जन्म दिया।
1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो उसने जनसंघ की वैचारिक और संगठनात्मक विरासत को आगे बढ़ाया। इस दृष्टि से अक्टूबर 1951 भारतीय राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक दूरदर्शी और रणनीतिक कदम था। इसने राष्ट्रवादी विचारधारा को स्थायी राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित किया और भारत की लोकतांत्रिक संरचना को स्थायी रूप से प्रभावित किया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु (23 जून 1953)
23 जून 1953 को श्रीनगर में नजरबंदी के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। आधिकारिक रूप से इसे हृदयाघात बताया गया, किंतु गिरफ्तारी, नजरबंदी, चिकित्सकीय देखभाल और पोस्टमार्टम की अनुपस्थिति ने दशकों तक विवाद को जीवित रखा।
उस समय वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे। जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के उनके अभियान ने उन्हें शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नेहरू की कश्मीर नीति से सीधे टकराव में ला दिया।
गिरफ्तारी और नजरबंदी
मई 1953 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था का विरोध करते हुए बिना अनुमति प्रवेश किया। यह एक सुनियोजित नागरिक अवज्ञा का कदम था।
उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर श्रीनगर में नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान—
-
उनकी गतिविधियों और संचार पर नियंत्रण रखा गया।
-
बाद में सीने में दर्द की शिकायतों की सूचना सामने आई।
-
परिवार और पार्टी सहयोगियों से मिलने की अनुमति सीमित थी।
समर्थकों का आरोप था कि उनकी चिकित्सकीय स्थिति को आवश्यक गंभीरता नहीं दी गई।
बीमारी और आधिकारिक कारण
22–23 जून 1953 की रात उन्हें गंभीर सीने में दर्द हुआ। चिकित्सकीय उपचार दिया गया, किंतु 23 जून की सुबह उनका निधन हो गया।
सरकारी घोषणा के अनुसार मृत्यु का कारण “मायोकार्डियल इन्फार्क्शन” (हृदयाघात) था। एक चिकित्सकीय बोर्ड ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया। किंतु स्वतंत्र पोस्टमार्टम न होने के कारण संदेह बना रहा।
विवाद के मुख्य बिंदु
पोस्टमार्टम का अभाव:
हिरासत में एक राष्ट्रीय नेता की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम न होना पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े करता है।
चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप:
कुछ आलोचकों का मत था कि विशेष उपचार या बेहतर सुविधा में स्थानांतरण में देरी हुई। यद्यपि इसे साजिश सिद्ध नहीं किया गया, पर प्रश्न अनुत्तरित रहे।
राजनीतिक संदेह:
उनकी बढ़ती राजनीतिक भूमिका और कश्मीर नीति के विरोध के कारण राजनीतिक आशंकाएँ व्यक्त की गईं, हालांकि किसी जांच में हत्या का ठोस प्रमाण सामने नहीं आया।
ऐतिहासिक प्रभाव
उनकी मृत्यु के दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुए—
-
भारतीय जनसंघ की वैचारिक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।
-
अनुच्छेद 370 के विरोध को नई गति मिली।
-
वे राष्ट्रवादी राजनीतिक विमर्श में प्रतीकात्मक व्यक्तित्व बन गए।
उनका निधन केवल एक घटना नहीं रहा; यह स्वतंत्र भारत में विपक्ष की राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
सवाल जो अब भी जीवित हैं
आधिकारिक रूप से उनकी मृत्यु प्राकृतिक मानी गई, किंतु पारदर्शिता की कमी—विशेषकर पोस्टमार्टम न होने—ने संदेह को जीवित रखा।
सात दशकों से अधिक समय बाद भी यह प्रकरण एक महत्वपूर्ण सीख देता है: जब किसी राजनीतिक नेता की हिरासत में मृत्यु होती है, तो पारदर्शिता केवल न्याय के लिए ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए भी अनिवार्य होती है।
इतिहास अधूरी कहानियों को भूलता नहीं। वह उन्हें शांतिपूर्वक संजोए रखता है—जब तक सत्य पूरी स्पष्टता के साथ सामने न आ जाए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुले रणक्षेत्र में नहीं, बल्कि हिरासत में दिवंगत हुए—एक ऐसे राष्ट्र की निगरानी में, जो अभी लोकतंत्र के अर्थ को समझ ही रहा था। वे कश्मीर में एकता का संदेश लेकर गए थे, किंतु ऐसे उत्तर के बिना लौटे, जो देश की अंतरात्मा को संतुष्ट कर पाता।
अनुत्तरित प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं, नैतिक भी हैं। जब किसी राष्ट्रीय नेता की मृत्यु बिना पारदर्शी जांच के होती है, तो संदेह समय के साथ समाप्त नहीं होता—वह और गहरा हो जाता है। लोकतंत्र प्रश्नों से कमजोर नहीं होता; वह मौन से कमजोर होता है।
चाहे कोई उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं, सिद्धांत स्पष्ट है—कोई भी नागरिक, विशेषकर जनप्रतिनिधि, अनिश्चितता की छाया में इस संसार से विदा नहीं होना चाहिए।
जब तक अंतिम प्रश्न का ईमानदार उत्तर नहीं मिलता, उनकी अंतिम यात्रा केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं रहेगी; वह इस बात की निरंतर याद दिलाती रहेगी कि सत्य ही किसी भी गणराज्य की वास्तविक आधारशिला है।